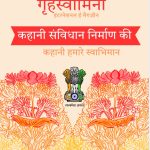इसोफ़ेगस
रात की पार्टी के बाद शिखा बेसुध पड़ी थी, बार्नेट अस्पताल के इमर्जेन्सी वार्ड की कुर्सी में। एक्यूट डीहाइड्रेशन। फिंचली मेमोरियल अस्पताल के वॉक-इन-सेंटर में नर्स ने शुरुआती जाँच-पड़ताल में ही अमित से कह दिया था, “शरीर पानी भी नहीं रोक पा रहा है, फ़्लूइड चढ़ाना होगा – बार्नेट के आपातकालीन वार्ड में ले जाइए। यहाँ यह सुविधा नहीं है।”
अमित और शिखा लंदन के सेंट्रल फिंचली इलाके में रहते थे। दोनों एक ही ऑफ़िस में काम करते थे, मित्रता प्यार में बदली और फिर दोनों संग रहने लगे। अमित ने गूगल मेप देखा, बार्नेट अस्पताल नज़दीक था तो गाड़ी का रुख़ वहीं किया। घर से अस्पताल तक की दस मिनिट की ड्राइव में ही शिखा ने दो और उल्टियाँ कर दीं। उल्टी भी क्या गला खिंच-खिंच के केवल पित्त ही पित्त निकल रहा था।
शिखा अंदर पहुँचते ही प्रतीक्षाकक्ष के बाथरूम की पास वाली सीट पर बैठ गयी। अपने अंदर उसे फिर एक मतली का माहौल बनता महसूस हो रहा था। अमित ने काउन्टर पर केस का ब्यौरा लिखवाया। तीन-चार मरीज़ों के बाद ही नाम आ गया। सलाइन चढ़ाने का केस था, मेडिकल के हिसाब से बहुत गंभीर बात नहीं थी, सो बिस्तर नहीं मिला। एक विंग में आरामदेह कुर्सियों में बैठे कुछ और मरीज़ों को सलाइन की बोतलें चढ़ रही थीं। इस तरह के मौकों पर शिखा को भारत की याद आ जाती थी। उसने सोचा, “पैसे ज़रूर लगते लेकिन प्राइवेट वॉर्ड में एक बेड मिल जाता!”
शिखा का सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसे कुर्सी में बैठना ज़रा न भा रहा था। असिस्टेंट डॉक्टर से पलंग की दरख़्वास्त की लेकिन कोई पलंग ख़ाली नहीं था। ख़ैर, बैठे-बैठे ही फ़्लूइड चढ़ाया गया। कुछ बूँदें शरीर में जाने के बाद उसे कुछ जान सी महसूस हुई। अब शरीर को तो पानी की मात्रा मिलने लगी थी लेकिन गले का सूखापन ज्यों का त्यों। जब तक गले से पानी की बूँद न सरके, प्यास कभी बुझती है भला! ये बात शिखा बहुत अच्छे से जानती थी!
“शिखू, पानी पिला दे, बेटा। थोड़ा सा पानी। बस दो-तीन बूँद”
पापा का पानी की दो-तीन, दो-तीन बूँदों के लिये हफ़्तों गिड़गिड़ाना शिखा की आँखों के आगे झूल गया।
पीड़ा की स्मृति से कुछ देर को तो मुक्ति मिलेगी! यही चाह थी शिखा को। इसलिए वह अपनी सीमा से बहुत ज़्यादा वाइन पी गई थी। और उसकी यह चाह उसे सूखे गले वाले पापा के एकदम समीप खींच लायी। कैसे मुक्त हुआ जा सकता है स्मृतियों से!
रात भर नींद न होने के कारण शिखा का सिर ज़ोर से भन्ना रहा था। सिर पर जैसे हथौड़े चल रहे हों। आँखें मुँद गयीं और प्यास, … उसकी खुद की नहीं – पापा की, जो उसके गले में आकर बैठ गयी। शिखा की आँखों से आँसू झरने को हुए पर नहीं आए। अपनी ही दी हुयी सलाह उसे याद आ गयी, “पापा, रोना मत, और पानी निकल जाएगा शरीर से।”
उन दिनों में जब भी पापा का ध्यान बँटाना असंभव हो जाता था, शिखा अस्पताल के कमरे का टी.वी. शुरू कर देती। टी.वी. वह तब भी शुरू कर लेती थी जब पापा गहरी नींद में रहते थे। उन दिनों एक विशेष समाचार ने उसका ध्यान आकर्षित किया हुआ था – जैन मुनि शिखर सागर के दिन पर दिन गिरते स्वास्थ्य का। आचार्य श्री को फेफड़ों का कैंसर था। अंदेशा था उनके जल्दी ही सल्लेखना के निश्चय की घोषणा का।
धार्मिक परिवार में शिखा का जन्म हुआ, पर वो कभी पूजा-पाठ-मंदिर वाली नहीं रही। जब तक भारत में थी तब तक तो साल में एकाध बार देव-दर्शन का निमित्त बन जाता, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद न ऐसा कोई संयोग बना और न ही उसने कोशिश की। पापा से ही मंदिरों के जीर्णोद्धार और आचार्यों के विहार और चौमासे की बातें सुनती रहती थी। पुणे के अस्पताल में इस ख़बर ने उसके बचपन की कई स्मृतियों को हिलोर दिया।
“मंदिर जाने-न जाने से आध्यात्म का कोई लेना-देना नहीं, पापा। मैं मंदिर जाने वालों से ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ।” जब भी पापा उसे देव-दर्शन की याद दिलाते, वह उन्हें यह डायलॉग चिपका देती। पापा अपना सा मुँह लेकर रह जाते पर भरपाई के लिए दो-चार संबंधित खबरें या कोई पौराणिक कथा सुना देते।
सल्लेखना के सिद्धांत को शिखा बचपन से सुनती आ रही थी। पापा ने ही समझाया था कि “मृत्यु जब द्वार पर आ जाए तो उसे सहजता से स्वीकार करना ही पौरुष है। मृत्यु को अनिवार्य और अपरिहार्य जानकर स्वेच्छा से सामर्थ्य के अनुसार धीरे-धीरे भोजन-पानी त्याग कर समाधि-मरण के लिए तैयार होना सल्लेखना है।”
साल होने को आया पापा को गुज़रे। दिन तो निकल जाता है, पर पापा का कराहना शिखा की रातों को अब भी खलबला देता है। गले से पेट तक जाने वाली लंबी नली इसोफ़ेगस से खाना-पानी पेट तक पहुँचता है। इसी का कैंसर हुआ था पापा को। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, शिखा आज भी खुद से यही तर्क-वितर्क करती रहती है।
“न, न – सिगरेट, शराब, तंबाकू किसी का व्यसन नहीं था उन्हें। डॉक्टरों को भी ताज्जुब हुआ कि पापा को यह कैंसर कैसे हो गया? पता नहीं, कैसे हो जाती है यह बीमारी!”
“दुख, नहीं दुख तो ऐसा कोई नहीं था। पापा तो बहुत ज़िंदादिल इंसान थे। दिल खोल कर हँसते थे। ज़ोर-ज़ोर से हा-हा-हा। शायद जेनेटिक था!, दादी को था न – पेट का कैंसर।”
“बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जैसे कोई-कोई पेड़ नहीं होते – काटते जाओ फिर बढ़ने लगते हैं, फिर काटो, फिर बढ़ेंगे, कितना भी काटते रहो- फिर-फिर बढ़ेंगे।”
“पूरी नली ही तो निकाल के अलग कर दी थी पापा की। ट्यूब से सब कुछ डालते थे। लगता था अब सब ठीक हो गया, लेकिन कहाँ – दो साल ठीक रहा। फिर आ गया कैंसर – अब गले का था। मरता नहीं है।”
“जब इंसान दर्द में होता है तो उसे कुछ नहीं सूझता। इतना बेबस हो जाता है कि बस चुप हो जाता है। ये चुप्पी अलग क़िस्म की चुप्पी है। सिर्फ़ होंठों के सिलने वाली नहीं, बल्कि तकिये से आत्मा का दम घोंटने वाली चुप्पी।”
इस चुप्पी का अर्थ उसने पापा की मूक आँखों से सीखा था।
जब फिर कैंसर हुआ तो रेडिएशन फिर शुरू हो गए। गले में गहरा ज़ख्म। खाना-पानी डालने वाली नली वहीं से होकर जाती थी जहाँ पर कैंसर था। नली बार-बार निकल जाती थी। फिर-फिर वहीं से नली डालनी होती थी। क्या अजीब शय है न ज़िंदगी, यूँ तो इससे इतना लगाव, लेकिन कभी साँसों का होना असहनीय हो जाता है।
पापा पानी की बस कुछ बूँदें चाहते थे गले में तरावट के लिए। पानी मुँह में डालने से सीधे फेफड़ों में चला जाता था – खाँसी होती थी और फिर फेफड़ों का संक्रमण। हो भी गया था। लेकिन फिर भी शिखा एक-एक बूँद डाल देती थी।
पापा को लगभग बेहोशी की हालत में ही रखा जाने लगा। कैंसर यूनिट से एक विशेष ड्रग मिलती थी जिससे मरीज़ की शारीरिक-संवेदनाएँ मर जाएँ, साँस चलती रहे। ड्रग कहीं और नहीं मिलती थी। एक बार यूनिट में नहीं मिली तो पूरा शहर छान कर एक कर डाला शिखा ने। दवा हर दो-तीन घंटे में देनी होती थी। और सड़कों की ख़ाक छानते-छानते कई घंटे बीत गए। शिखा ने कहानियों में सुना था, सात नरक होते हैं। एक नरक ऐसा होता है जिसमें सारे समुद्रों का पानी पी लेने के बाद भी प्यास ज्यों की त्यों बनी रहती है। आज सातों नरकों की बारी थी शायद।
शाम होते-होते किसी एक एन.जी.ओ. से कुछ डोज़ मिल पाए। डोज़ मिलते ही शिखा की जान में जान आयी। पापा के जीवन की डोर उसके हाथों में थी। “पापा, पापा, … ” रुँधे गले से दबी आवाज में वह वहीं चीखी “दवा मिल गयी, पापा, बस मैं आ रही हूँ!”
तेज़ क़दमों से वह पापा के वॉर्ड में पहुँची। टी. वी. चल रहा था। मुनि महाराज की सल्लेखना की खबर आ रही थी। उन्होंने अन्न-जल स्वेच्छा से छोड़ दिया था। कष्ट तो वैसा ही होगा उन्हें भी जैसे पापा को था। लेकिन शांत मुद्रा में दिखाई देते थे, माहौल आँसुओं से भीगा पर उत्सव का सा था। पापा की नज़रें टी. वी. की तरफ़ थीं, पापा ने शिखा की ओर देखा और जैसे अनुनय भरी आँखों से कुछ कहा। शिखा घबरा कर बाहर आ गयी। अपने आप को किसी तरह संभाल कर उसने लंदन अमित को फ़ोन लगाया,
“हैलो, अमित। वो दवा मिल गई है। … लेकिन, लेकिन मैं नर्स से बोल सकती हूँ कि नहीं मिली।
… दर्द का अंत ज़रूरी है, अमित। अब देखा नहीं जाता।”
फ़ोन ने कुछ देर दोनों की ख़ामोश साँसें सुनी। कोई ऐसी बात हुयी जो बिना कहे सुनी जानी थी।
उस मूक वार्तालाप के कुछ सेकेण्ड्स बाद ही लाइन कट हो गयी।
वार्ड में बैठे-बैठे शिखा की आँख लग गयी थी। अचानक उसकी नींद टूटी और उसे महसूस हुआ कि उसके माथे पर कोई हाथ फेर रहा था, वह अमित था। “जूस पी लो, शिखा! देखो, सलाइन की बॉटल आधी ख़ाली हो चुकी है।अब तुम ठीक हो रही हो, अब निश्चिंत होकर पी सकती हो।”
शिखा को एहसास हुआ, उसकी इसोफ़ेगस भीग रही थी।अब उसने आँसुओं को बह जाने दिया।
ऋचा जैन
ब्रिटेन